शब्द विचार: हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है जो शब्दों के स्वरूप, उनके प्रकार, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। शब्द विचार के माध्यम से हम शब्दों के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं और उनका सही प्रयोग सीखते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उनकी परिभाषाएँ और उदाहरण शामिल होते हैं।
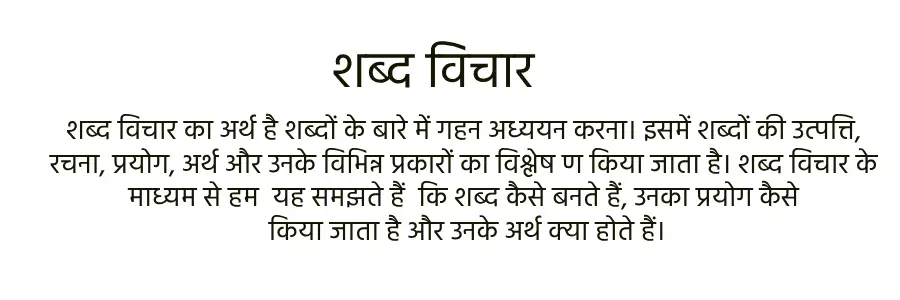
शब्द विचार क्या होता है?
शब्द विचार का अर्थ है शब्दों के बारे में गहन अध्ययन करना। इसमें शब्दों की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग, अर्थ और उनके विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण किया जाता है। शब्द विचार के माध्यम से हम यह समझते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है और उनके अर्थ क्या होते हैं।
शब्द क्या होते हैं?(Shabd kise kahate hain)
शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं जो अर्थपूर्ण होते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और इनका प्रयोग वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, “राम”, “खेल”, “किताब” आदि शब्द हैं।
शब्द और पद क्या हैं?
- शब्द: शब्द वर्णों के मेल से बनने वाली वह इकाई है जो स्वतंत्र रूप से अर्थ रखती है। जैसे: “कमल”, “फूल”, “पानी”।
- पद: जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। पद वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है। जैसे: “राम ने खाना खाया” में “राम”, “खाना”, और “खाया” पद हैं।
शब्द विचार का वर्गीकरण/ भेद
शब्द विचार को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है:
- रचना (बनावट) के आधार पर
- प्रयोग के आधार पर
- उत्पत्ति के आधार पर
- अर्थ के आधार पर
रचना (बनावट) के आधार पर शब्द के भेद और उदाहरण(Shabd ke bhed aur udaaharan )
1. रूढ़ शब्द :
रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता।
रूढ़ शब्दों के उदाहरण:
– “कमल” (यह शब्द केवल एक विशेष फूल के लिए प्रयोग किया जाता है।)
– “गाय” (यह शब्द केवल एक विशेष पशु के लिए प्रयोग किया जाता है।)
रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ रूढ़ शब्दों के 20 उदाहरण दिए गए हैं:
- कमल – एक विशेष प्रकार का फूल।
- गाय – एक विशेष पशु।
- पानी – एक तरल पदार्थ।
- आग – जलने वाली वस्तु।
- सूरज – आकाश में चमकने वाला ग्रह।
- चाँद – रात में चमकने वाला उपग्रह।
- हाथी – एक विशाल जानवर।
- बंदर – एक प्रकार का जानवर।
- पेड़ – एक प्राकृतिक वनस्पति।
- फूल – पौधों का सुगंधित भाग।
- नदी – बहता हुआ जल।
- पहाड़ – ऊँची भूमि का भाग।
- आम – एक फल।
- किताब – ज्ञान का स्रोत।
- मकान – रहने का स्थान।
- रोटी – खाने की वस्तु।
- बादल – आकाश में दिखने वाला जलवाष्प।
- तारा – आकाश में चमकने वाली वस्तु।
- साँप – एक सरीसृप जानवर।
- मोर – एक पक्षी।
ये सभी शब्द रूढ़ शब्द हैं क्योंकि इनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता और ये किसी विशेष वस्तु, प्राणी या भाव को दर्शाते हैं।
2. यौगिक शब्द
यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और इनके टुकड़ों का अर्थ होता है।
यौगिक शब्दों के उदाहरण:
– “विद्यालय” (विद्या + आलय)
– “पंकज” (पंक + ज)
यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और इनके टुकड़ों का अर्थ होता है। यहाँ यौगिक शब्दों के 20 उदाहरण दिए गए हैं:
- विद्यालय – विद्या + आलय (ज्ञान का स्थान)
- पुस्तकालय – पुस्तक + आलय (किताबों का स्थान)
- रसोईघर – रसोई + घर (खाना बनाने का स्थान)
- जलज – जल + ज (पानी में पैदा होने वाला, कमल)
- दशानन – दश + आनन (दस मुख वाला, रावण)
- राजपुत्र – राज + पुत्र (राजा का पुत्र)
- गंगाजल – गंगा + जल (गंगा नदी का पानी)
- चंद्रमा – चंद्र + मा (चमकने वाला चंद्र)
- सूर्योदय – सूर्य + उदय (सूरज का निकलना)
- पथिक – पथ + इक (रास्ते पर चलने वाला)
- हिमालय – हिम + आलय (बर्फ का घर)
- नरेश – नर + ईश (मनुष्यों का स्वामी, राजा)
- धनवान – धन + वान (धन वाला)
- वनवास – वन + वास (जंगल में रहना)
- राजधानी – राज + धानी (राज्य की मुख्य नगरी)
- गुरुकुल – गुरु + कुल (गुरु का स्थान)
- जलधारा – जल + धारा (पानी की धारा)
- महाराज – महा + राज (बड़ा राजा)
- सत्यवादी – सत्य + वादी (सच बोलने वाला)
- प्राणदान – प्राण + दान (जीवन देना)
ये सभी शब्द यौगिक शब्द हैं क्योंकि ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं और इनके टुकड़ों का अर्थ होता है।
3. योगरूढ़ शब्द
योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्दों की तरह बनते हैं, लेकिन इनका अर्थ उनके टुकड़ों के अर्थ से अलग होता है।
योगरूढ़ शब्दों के उदाहरण:
– “दशानन” (दश + आनन) – यह रावण के लिए प्रयोग किया जाता है।
– “जलज” (जल + ज) – यह कमल के लिए प्रयोग किया जाता है।
- दशानन – दश + आनन (दस मुख वाला, रावण)
- जलज – जल + ज (पानी में पैदा होने वाला, कमल)
- पंकज – पंक + ज (कीचड़ में पैदा होने वाला, कमल)
- गजानन – गज + आनन (हाथी के समान मुख वाला, गणेश)
- नीलकंठ – नील + कंठ (नीले कंठ वाला, शिव)
- चक्रधर – चक्र + धर (चक्र धारण करने वाला, विष्णु)
- कमलनयन – कमल + नयन (कमल जैसे नेत्र वाला, विष्णु)
- त्रिलोचन – त्रि + लोचन (तीन नेत्र वाला, शिव)
- पीतांबर – पीत + अंबर (पीले वस्त्र धारण करने वाला, कृष्ण)
- महादेव – महा + देव (सबसे बड़े देवता, शिव)
- विषधर – विष + धर (विष धारण करने वाला, सर्प)
- कृष्णसार – कृष्ण + सार (काले रंग का सार, हिरण)
- श्वेतांबर – श्वेत + अंबर (सफेद वस्त्र धारण करने वाला, जैन मुनि)
- सहस्त्रबाहु – सहस्त्र + बाहु (हजार भुजाओं वाला, राजा सहस्त्रबाहु)
- कुंडलधारी – कुंडल + धारी (कुंडल पहनने वाला, कृष्ण)
- चतुर्भुज – चतुर + भुज (चार भुजाओं वाला, विष्णु)
- मृगांक – मृग + अंक (चंद्रमा)
- किरीटी – किरीट + ई (मुकुट धारण करने वाला, अर्जुन)
- शंखधर – शंख + धर (शंख धारण करने वाला, विष्णु)
- गदाधर – गदा + धर (गदा धारण करने वाला, विष्णु)
ये सभी शब्द योगरूढ़ शब्द हैं क्योंकि ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, लेकिन इनका अर्थ उनके टुकड़ों के अर्थ से अलग होता है।
प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और उदाहरण
1. विकारी शब्द :
विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदलता है।
विकारी शब्दों के उदाहरण:
– “लड़का” (लड़का, लड़के, लड़कों)
– “किताब” (किताब, किताबें)
- लड़का
- लड़की
- किताब
- पेड़
- माता
- पिता
- गाय
- बैल
- स्कूल
- फूल
- नदी
- पर्वत
- बच्चा
- बच्ची
- शहर
- गाँव
- मित्र
- सखी
- कुत्ता
- बिल्ली
ये शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं।
उदाहरण:
- लड़का (एकवचन) → लड़के (बहुवचन)
- किताब (स्त्रीलिंग) → किताबें (बहुवचन)
- गाय (स्त्रीलिंग) → गायें (बहुवचन)
विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शामिल होते हैं।
2. अविकारी शब्द :
अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता।
अविकारी शब्दों के उदाहरण**:
– “और”, “पर”, “किन्तु”, “अतः”
- और
- पर
- अगर
- क्योंकि
- यदि
- ताकि
- इसलिए
- किंतु
- परंतु
- बल्कि
- जब
- तब
- कब
- कहाँ
- वहाँ
- यहाँ
- धीरे
- तेज
- अच्छा
- बुरा
अविकारी शब्दों में क्रिया-विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक शब्द शामिल होते हैं।
उदाहरण:
- वह धीरे चलता है। (क्रिया-विशेषण)
- मैं और तुम जाएंगे। (समुच्चयबोधक)
- वह घर पर है। (संबंधबोधक)
- अरे! यह क्या हुआ? (विस्मयादिबोधक)
ये शब्द किसी भी स्थिति में अपना रूप नहीं बदलते।
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद और उदाहरण
1. तत्सम शब्द :
तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
तत्सम शब्दों के उदाहरण:
– “अग्नि”, “विद्या”, “सूर्य”
- अग्नि
- वायु
- जल
- पृथ्वी
- सूर्य
- चंद्र
- नदी
- पर्वत
- आशा
- क्रोध
- मित्र
- धन
- विद्या
- कर्म
- यज्ञ
- गुरु
- शिष्य
- राजा
- रानी
- धर्म
तत्सम शब्दों का प्रयोग अक्सर साहित्य, धार्मिक ग्रंथों और औपचारिक भाषा में किया जाता है।
उदाहरण:
- अग्नि में आहुति दी गई।
- वायु के बिना जीवन संभव नहीं है।
- सूर्य प्रकाश का स्रोत है।
- विद्या से व्यक्ति महान बनता है।
ये शब्द संस्कृत के मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
2. तद्भव शब्द :
तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, लेकिन इनमें समय के साथ कुछ परिवर्तन हो गया है। ये शब्द अपने मूल रूप में नहीं रहते, बल्कि थोड़े बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
तद्भव शब्दों के उदाहरण:
– “आग” (अग्नि), “सूरज” (सूर्य)
- आग (अग्नि से)
- हवा (वायु से)
- पानी (जल से)
- सूरज (सूर्य से)
- चाँद (चंद्र से)
- नदिया (नदी से)
- पहाड़ (पर्वत से)
- आस (आशा से)
- रोष (क्रोध से)
- मित्तर (मित्र से)
- धन (धन से, लेकिन उच्चारण में परिवर्तन)
- पढ़ाई (विद्या से)
- काम (कर्म से)
- जज्ञ (यज्ञ से)
- गुरु (गुरु से, लेकिन उच्चारण में परिवर्तन)
- राज (राजा से)
- रान (रानी से)
- धरम (धर्म से)
- घर (गृह से)
- मुँह (मुख से)
तद्भव शब्दों का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में अधिक होता है।
उदाहरण:
- आग से सावधान रहना चाहिए।
- हवा तेज चल रही है।
- सूरज निकल आया है।
- चाँद रात में चमकता है।
ये शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से विकसित हुए हैं, लेकिन इनका रूप बदल गया है।
3. देशज शब्द
देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय या स्थानीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं। ये शब्द संस्कृत या अन्य भाषाओं से नहीं लिए गए हैं, बल्कि सीधे स्थानीय बोलियों और भाषाओं से हिंदी में शामिल हुए हैं।
देशज शब्दों के उदाहरण:
– “ठेला”, “लोटा”
- खिड़की
- लोटा
- झोपड़ी
- थाली
- चूल्हा
- पगड़ी
- डिब्बा
- गुड़िया
- टोकरी
- खुरपी
देशज शब्दों का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में अधिक होता है और ये शब्द हिंदी भाषा को सरल और सहज बनाते हैं।
उदाहरण:
- खिड़की से हवा आ रही है।
- लोटा में पानी भर लो।
- झोपड़ी में रहने वाले लोग गरीब होते हैं।
- थाली में खाना परोसो।
ये शब्द हिंदी भाषा की सहजता और सरलता को दर्शाते हैं।
4. विदेशी/विदेशज शब्द
विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो अन्य भाषाओं (जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की आदि) से हिंदी में आए हैं। ये शब्द हिंदी भाषा में इस तरह शामिल हो गए हैं कि अब ये आम बोलचाल का हिस्सा बन चुके हैं।
विदेशी/विदेशज शब्दों के उदाहरण:
– “स्कूल” (अंग्रेजी), “किताब” (अरबी)
- अंग्रेजी से:
- टेबल (Table)
- पेन (Pen)
- स्कूल (School)
- फारसी से:
- जमीन (ज़मीन)
- दुकान (दुकान)
- किताब (किताब)
- अरबी से:
- दुनिया (दुनिया)
- कलम (क़लम)
- हिसाब (हिसाब)
- पुर्तगाली से:
- अलमारी (Almari)
- चाबी (Chave)
- तुर्की से:
- बारूद (Barut)
विदेशी शब्दों का प्रयोग आम बोलचाल और लिखित भाषा में व्यापक रूप से होता है।
उदाहरण:
- टेबल पर किताब रख दो।
- दुकान से सामान ले आओ।
- कलम से लिखो।
- अलमारी में कपड़े रखे हैं।
ये शब्द हिंदी भाषा को समृद्ध और विविधतापूर्ण बनाते हैं।
अर्थ के आधार पर शब्द के भेद उदाहरण सहित
1. एकार्थक शब्द :
एकार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। यानी ये शब्द किसी एक विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान, या भाव को ही व्यक्त करते हैं।
एकार्थक शब्दों के उदाहरण:
– “सूरज”, “चाँद”
- सूर्य – सूर्य का अर्थ केवल सूरज होता है।
- चंद्रमा – चंद्रमा का अर्थ केवल चाँद होता है।
- पृथ्वी – पृथ्वी का अर्थ केवल धरती होता है।
- नदी – नदी का अर्थ केवल नदी होता है।
- पर्वत – पर्वत का अर्थ केवल पहाड़ होता है।
- आकाश – आकाश का अर्थ केवल आसमान होता है।
- वायु – वायु का अर्थ केवल हवा होता है।
- अग्नि – अग्नि का अर्थ केवल आग होता है।
- जल – जल का अर्थ केवल पानी होता है।
- गुरु – गुरु का अर्थ केवल शिक्षक या आचार्य होता है।
उदाहरण वाक्य:
- सूर्य प्रतिदिन पूर्व दिशा से निकलता है।
- चंद्रमा रात में चमकता है।
- पृथ्वी पर जीवन संभव है।
- नदी का पानी स्वच्छ होना चाहिए।
- पर्वत की चोटी बर्फ से ढकी हुई है।
एकार्थक शब्दों का प्रयोग स्पष्टता और सटीकता के लिए किया जाता है, क्योंकि इनका केवल एक ही अर्थ होता है।
2. अनेकार्थक शब्द :
अनेकार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। यानी ये शब्द अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग अर्थ देते हैं।
अनेकार्थक शब्दों के उदाहरण:
– “कल” (समय के लिए और मशीन के लिए)
– “अंक” (संख्या और गोद)
- कल
- अर्थ 1: आने वाला दिन (जैसे: कल मैं दिल्ली जाऊँगा।)
- अर्थ 2: बीता हुआ दिन (जैसे: कल मैंने फिल्म देखी थी।)
- पत्र
- अर्थ 1: चिट्ठी (जैसे: उसने मुझे एक पत्र लिखा।)
- अर्थ 2: पेड़ की पत्ती (जैसे: यह पेड़ हरे पत्रों से भरा है।)
- फल
- अर्थ 1: खाने वाला फल (जैसे: सेब एक मीठा फल है।)
- अर्थ 2: परिणाम (जैसे: मेहनत का फल मिलता है।)
- हार
- अर्थ 1: गले का आभूषण (जैसे: उसने सोने का हार पहना।)
- अर्थ 2: पराजय (जैसे: टीम को हार का सामना करना पड़ा।)
- अंक
- अर्थ 1: संख्या (जैसे: यह अंक बहुत बड़ा है।)
- अर्थ 2: गोद (जैसे: माँ ने बच्चे को अंक में ले लिया।)
- काम
- अर्थ 1: कार्य (जैसे: उसका काम बहुत अच्छा है।)
- अर्थ 2: इच्छा या वासना (जैसे: काम, क्रोध, और लोभ मनुष्य के शत्रु हैं।)
- मत
- अर्थ 1: राय (जैसे: आपका मत क्या है?)
- अर्थ 2: वोट (जैसे: चुनाव में मत डालना जरूरी है।)
- सूरज
- अर्थ 1: सूर्य (जैसे: सूरज पूर्व में उगता है।)
- अर्थ 2: एक प्रकार का पक्षी (जैसे: सूरजमुखी पक्षी बहुत सुंदर होता है।)
- धन
- अर्थ 1: पैसा (जैसे: धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता।)
- अर्थ 2: तीर (जैसे: धनुष और धन से युद्ध किया जाता है।)
- कर्ण
- अर्थ 1: कान (जैसे: उसके कर्ण बहुत तेज हैं।)
- अर्थ 2: महाभारत का एक पात्र (जैसे: कर्ण एक महान योद्धा थे।)
उदाहरण वाक्य:
- कल मैं दिल्ली जाऊँगा। (आने वाला दिन)
कल मैंने फिल्म देखी थी। (बीता हुआ दिन) - उसने मुझे एक पत्र लिखा। (चिट्ठी)
यह पेड़ हरे पत्रों से भरा है। (पत्तियाँ) - सेब एक मीठा फल है। (खाने वाला फल)
मेहनत का फल मिलता है। (परिणाम)
अनेकार्थक शब्दों का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल जाता है, इसलिए इनका प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
3. पर्यायवाची शब्द :
पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं।
पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण:
– “सूरज” – “रवि”, “दिनकर”
– “पानी” – “जल”, “नीर”
- सूरज – सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, प्रभाकर
- पानी – जल, नीर, सलिल, वारि, अंबु
- आग – अग्नि, पावक, अनल, धूमकेतु, हुताशन
- पहाड़ – पर्वत, गिरि, अचल, भूधर, शैल
- हवा – वायु, पवन, समीर, अनिल, मरुत
- चाँद – चंद्रमा, सोम, शशि, राकेश, निशाकर
- पृथ्वी – धरती, भूमि, वसुंधरा, धरा, अवनि
- नदी – सरिता, तटिनी, निर्झर, दरिया, स्रोतस्विनी
- आकाश – गगन, अंबर, नभ, व्योम, आसमान
- कमल – पंकज, नीरज, सरोज, अरविंद, जलज
ये शब्द हिंदी भाषा में समानार्थी शब्दों के उदाहरण हैं।
4. विलोम शब्द :
विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक-दूसरे के विपरीत होते हैं।
विलोम शब्दों के उदाहरण:
– “दिन” – “रात”
– “सुख” – “दुख”
- दिन – रात
- सुख – दुख
- जीवन – मृत्यु
- उजाला – अंधेरा
- सत्य – असत्य
- लाभ – हानि
- आशा – निराशा
- जय – पराजय
- गर्मी – सर्दी
- ऊपर – नीचे
ये शब्द हिंदी भाषा में विपरीतार्थक शब्दों के उदाहरण हैं।
शब्द विचार का महत्व क्या है?
शब्द विचार का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें शब्दों के सही प्रयोग, उनके अर्थ और उनकी उत्पत्ति के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। यह भाषा को सही ढंग से समझने और प्रयोग करने में मदद करता है।
शब्द समूह के लिए एक शब्द :
– “जो पढ़ता है” – “पाठक”
– “जो लिखता है” – “लेखक”
पशु पक्षियों की बोलियां :
– “कुत्ता” – “भौंकना”
– “बिल्ली” – “म्याऊँ”
अन्य ध्वनियां :
– “बारिश” – “टप-टप”
– “हवा” – “सर-सर”
शब्द विचार से संबंधित महत्वपूर्ण FAQs
1. शब्द विचार क्यों महत्वपूर्ण है?
शब्द विचार भाषा को सही ढंग से समझने और प्रयोग करने में मदद करता है।
2. रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द में क्या अंतर है?
रूढ़ शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, जबकि यौगिक शब्दों के टुकड़ों का अर्थ होता है।
3. तत्सम और तद्भव शब्द क्या हैं?
तत्सम शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं, जबकि तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं लेकिन इनमें परिवर्तन हुआ है।
4. विलोम शब्द क्या होते हैं?
विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक-दूसरे के विपरीत होते हैं।
