भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और सबसे बड़ी इकाई वाक्य। वाक्य विचार हिंदी व्याकरण का वह महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें सिखाता है कि शब्दों को किस प्रकार व्यवस्थित करके सार्थक और प्रभावी विचार अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। एक अच्छा वाक्य ही संचार की सफलता की कुंजी है।
वाक्य की परिभाषा, भेद, उदाहरण (vaaky kee paribhaasha, bhed, udaaharan)
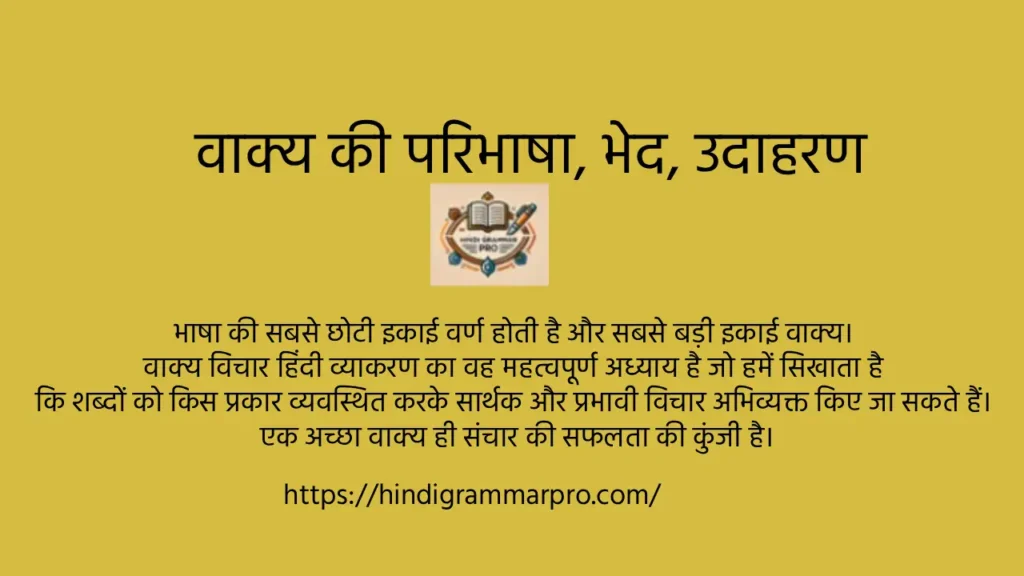
वाक्य की परिभाषा:
वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह है जिससे कोई पूर्ण अर्थ निकलता है। वाक्य के लिए तीन बातें आवश्यक हैं:
१. सार्थकता – शब्दों का अर्थपूर्ण होना
२. पूर्णता – विचार की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति
३. योग्य क्रम – शब्दों का उचित क्रम में व्यवस्थित होना
उदाहरण: “राम पुस्तक पढ़ता है” एक सार्थक वाक्य है जबकि “पढ़ता राम पुस्तक है” निरर्थक शब्द समूह है।
वाक्य के भेद:
१. अर्थ के आधार पर वाक्य भेद (Types of Sentences Based on Meaning)
भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति के तरीके के आधार पर वाक्यों के चार मुख्य भेद किए जाते हैं। यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य किस उद्देश्य से बोला या लिखा जा रहा है।
१. विधानवाचक वाक्य (Declarative or Assertive Sentences)
परिभाषा: जिस वाक्य से किसी तथ्य, सूचना, विचार, अनुभव, या घटना का वर्णन या कथन प्रकट हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का उद्देश्य किसी बात की जानकारी देना होता है, प्रश्न पूछना या आज्ञा देना नहीं। इन वाक्यों के अंत में पूर्णविराम (.) का प्रयोग होता है।
विशेषताएँ:
- ये वाक्य किसी बात की ‘सूचना’ देते हैं।
- इनमें तथ्यात्मकता होती है।
- वाक्य का अंत पूर्णविराम (.) से होता है।
उदाहरण और विश्लेषण (क्यों है विधानवाचक?):
- “आज खूब बारिश हो रही है।”
- विश्लेषण: यह वाक्य एक तथ्य और सूचना दे रहा है कि मौसम की क्या स्थिति है। यह न तो कोई प्रश्न है और न ही आज्ञा।
- “मैंने एक नई कार खरीदी है।”
- विश्लेषण: यह वाक्य वक्ता के एक व्यक्तिगत अनुभव या क्रिया के बारे में बता रहा है। इसका उद्देश्य सूचना देना है।
- “सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है।”
- विश्लेषण: यह वाक्य एक सार्वभौमिक सत्य का वर्णन कर रहा है, जो एक तथ्य है।
- “गाय एक दूध देने वाला पशु है।”
- विश्लेषण: यह वाक्य जानकारी दे रहा है। यह गाय की परिभाषा बता रहा है।
- “वह हर दिन व्यायाम करता है।”
- विश्लेषण: यह वाक्य किसी की दिनचर्या के बारे में एक तथ्य बता रहा है।
- “यह पुस्तक बहुत रोचक है।”
- विश्लेषण: यह वाक्य वक्ता की राय या विचार व्यक्त कर रहा है।
- “कल स्कूल में छुट्टी है।”
- विश्लेषण: यह वाक्य भविष्य की एक सूचना दे रहा है।
- “उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।”
- विश्लेषण: यह वाक्य एक घटना के परिणाम का वर्णन कर रहा है।
- “भारत की राजधानी नई दिल्ली है।”
- विश्लेषण: यह वाक्य एक भौगोलिक तथ्य की जानकारी दे रहा है।
- “मेरा मित्र बहुत अच्छा गाता है।”
- विश्लेषण: यह वाक्य किसी की क्षमता के बारे में एक कथन कर रहा है।
२. प्रश्नवाचक वाक्य (Interrogative Sentences)
परिभाषा: जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का उद्देश्य किसी से कुछ जानना या पूछताछ करना होता है। इनके अंत में प्रश्नवाचक चिह्न (?) लगाया जाता है।
विशेषताएँ:
- इन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता है।
- अक्सर ‘क्या’, ‘क्यों’, ‘कब’, ‘कहाँ’, ‘कैसे’, ‘कौन’ जैसे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है।
- वाक्य का अंत प्रश्नवाचक चिह्न (?) से होता है।
उदाहरण और विश्लेषण (क्यों है प्रश्नवाचक?):
- “तुम्हारा नाम क्या है?”
- विश्लेषण: यह वाक्य सीधे तौर पर एक प्रश्न पूछ रहा है (‘क्या’ शब्द का प्रयोग) ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके।
- “क्या तुम कल स्कूल जाओगे?”
- विश्लेषण: यह वाक्य ‘हाँ’ या ‘नहीं’ में उत्तर देने योग्य एक सरल प्रश्न है। (‘क्या’ से शुरू हो रहा है)।
- “तुम यह काम क्यों कर रहे हो?”
- विश्लेषण: यह वाक्य किसी कार्य के कारण के बारे में पूछताछ कर रहा है। (‘क्यों’ शब्द का प्रयोग)।
- “तुम्हारा जन्मदिन कब है?”
- विश्लेषण: यह वाक्य समय के बारे में एक प्रश्न है। (‘कब’ शब्द का प्रयोग)।
- “तुम कहाँ रहते हो?”
- विश्लेषण: यह वाक्य स्थान के बारे में जानकारी माँग रहा है। (‘कहाँ’ शब्द का प्रयोग)।
- “यह काम कैसे करता है?”
- विश्लेषण: यह वाक्य किसी विधि या तरीके के बारे में प्रश्न उठा रहा है। (‘कैसे’ शब्द का प्रयोग)।
- “इस पुस्तक को किसने लिखा?”
- विश्लेषण: यह वाक्य कर्ता के बारे में पूछ रहा है। (‘किसने’ शब्द का प्रयोग)।
- “क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ?”
- विश्लेषण: यह एक विनम्र प्रश्न है जो सहायता की पेशकश के रूप में पूछा गया है।
- “तुमने यह निर्णय कब लिया?”
- विश्लेषण: यह वाक्य किसी निर्णय के समय के बारे में जानना चाहता है।
- “क्या तुम्हें यह फिल्म पसंद आई?”
- विश्लेषण: यह वाक्य किसी की राय जानने के लिए एक सीधा प्रश्न है।
३. आज्ञावाचक वाक्य (Imperative Sentences)
परिभाषा: जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, उपदेश, प्रार्थना, या अनुरोध का भाव प्रकट हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में कर्ता ‘तुम’ या ‘आप’ छिपा रहता है, जिसे ‘लुप्त कर्ता’ कहते हैं।
विशेषताएँ:
- इनमें आदेश, अनुरोध या प्रार्थना का भाव होता है।
- कर्ता प्रायः छिपा (लुप्त) रहता है।
- वाक्य का अंत पूर्णविराम (.) या विस्मयादिबोधक चिह्न (!) से हो सकता है।
उदाहरण और विश्लेषण (क्यों है आज्ञावाचक?):
- “कृपया शांत बैठिए।”
- विश्लेषण: यह वाक्य एक विनम्र अनुरोध या प्रार्थना व्यक्त कर रहा है। (‘कृपया’ शब्द का प्रयोग)।
- “जाकर पानी लाओ।”
- विश्लेषण: यह वाक्य एक सीधा आदेश दे रहा है। (लुप्त कर्ता ‘तुम’)।
- “कभी झूठ न बोलो।”
- विश्लेषण: यह वाक्य एक उपदेश या सलाह दे रहा है।
- “अपना काम स्वयं करो।”
- विश्लेषण: यह वाक्य सीख दे रहा है, यह एक आदेशात्मक सलाह है।
- “धीरे बोलो।”
- विश्लेषण: यह वाक्य एक निर्देश दे रहा है।
- “मेरी बात सुनो!”
- विश्लेषण: यह वाक्य एक कड़े आदेश का भाव व्यक्त कर रहा है। (विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग)।
- “रोज सुबह जल्दी उठा करो।”
- विश्लेषण: यह वाक्य एक अच्छी आदत के लिए सलाह दे रहा है।
- “काम खत्म होने तक यहाँ रुको।”
- विश्लेषण: यह वाक्य एक शर्तसहित आदेश दे रहा है।
- “मेरी帮助 करें।” (कृपया मेरी मदद करें।)
- विश्लेषण: यह वाक्य सहायता के लिए एक विनम्र प्रार्थना है।
- “चोरी करना पाप है।” (इसका निहित अर्थ है ‘चोरी मत करो’)
- विश्लेषण: यह वाक्य एक नैतिक उपदेश दे रहा है।
४. विस्मयादिबोधक वाक्य (Exclamatory Sentences)
परिभाषा: जिस वाक्य से आश्चर्य, हर्ष, शोक, क्रोध, भय, प्रशंसा आदि तीव्र मनोभावों का बोध हो, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मयादिबोधक शब्दों (जैसे- अरे!, वाह!, हाय!, ओह!) का प्रयोग होता है और अंत में विस्मयादिबोधक चिह्न (!) लगाया जाता है।
विशेषताएँ:
- इनमें अचानक उत्पन्न हुए तीव्र भाव व्यक्त होते हैं।
- विस्मयबोधक शब्दों का प्रयोग होता है।
- वाक्य का अंत विस्मयादिबोधक चिह्न (!) से होता है।
उदाहरण और विश्लेषण (क्यों है विस्मयादिबोधक?):
- “अरे! तुम यहाँ कब आए?”
- विश्लेषण: ‘अरे!’ शब्द अचानक और अन预期्मित मुलाकात पर आश्चर्य व्यक्त कर रहा है।
- “वाह! कितना सुन्दर दृश्य है!”
- विश्लेषण: ‘वाह!’ शब्द दृश्य की सुंदरता देखकर प्रशंसा और हर्ष के भाव व्यक्त कर रहा है।
- “हाय! मेरा फोन टूट गया!”
- विश्लेषण: ‘हाय!’ शब्द एक दुर्घटना पर दुःख और निराशा व्यक्त कर रहा है।
- “ओह! बहुत ठंड लग रही है!”
- विश्लेषण: ‘ओह!’ शब्द कष्ट या पीड़ा के भाव को दर्शा रहा है।
- “कितना भद्दा काम किया है तुमने!”
- विश्लेषण: यह वाक्य क्रोध और निंदा के भाव से भरा हुआ है (बिना विस्मयबोधक शब्द के भी)।
- “अच्छा! तो तुम ही हो जिसने यह किया!”
- विश्लेषण: ‘अच्छा!’ शब्द जानकारी मिलने पर आश्चर्य या कभी-कभी धमकी का भाव भी व्यक्त कर सकता है।
- “शाबाश! तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया!”
- विश्लेषण: ‘शाबाश!’ शब्द बधाई और प्रोत्साहन का भाव व्यक्त कर रहा है।
- “छि:! यहाँ कितनी गंदगी फैली है!”
- विश्लेषण: ‘छि:’ शब्द घृणा और अप्रसन्नता का भाव व्यक्त कर रहा है।
- “बचाओ! आग लग गई!”
- विश्लेषण: यह वाक्य भय और डर के तीव्र भाव को व्यक्त कर रहा है।
- “अहा! मैं परीक्षा में पास हो गया!”
- विश्लेषण: ‘अहा!’ शब्द खुशी और उत्साह के अत्यंत उत्साहपूर्ण भाव व्यक्त कर रहा है।
इस प्रकार, वाक्य के अंत में प्रयुक्त चिह्न और उसके भाव के आधार पर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई वाक्य अर्थ के आधार पर किस श्रेणी में आता है।
२. रचना के आधार पर वाक्य भेद (Types of Sentences Based on Structure)
वाक्य की बनावट और उसके घटकों की जटिलता के आधार पर वाक्यों के तीन मुख्य भेद किए जाते हैं। यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य में कितने उपवाक्य हैं और वे एक-दूसरे से कैसे जुड़े हैं।
१. सरल वाक्य (Simple Sentence)
परिभाषा: जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य (Subject) और केवल एक विधेय (Predicate) हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक ही क्रिया होती है और यह एक ही विचार को व्यक्त करता है। इसे ‘साधारण वाक्य’ भी कहा जाता है।
विशेषताएँ:
- इसमें केवल एक मुख्य क्रिया होती है।
- यह एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है।
- इसके दो टुकड़े नहीं किए जा सकते।
- इसमें कोई योजक (जैसे- और, परन्तु, कि) नहीं होता।
उदाहरण और विश्लेषण (क्यों है सरल वाक्य?):
- “बच्चा खेल रहा है।”
- विश्लेषण: इसमें एक कर्ता (‘बच्चा’) और एक ही क्रिया (‘खेल रहा है’) है। इसके दो भाग नहीं किए जा सकते।
- “पक्षी उड़ रहे हैं।”
- विश्लेषण: एक कर्ता (‘पक्षी’) और एक क्रिया (‘उड़ रहे हैं’)। यह एक पूर्ण और स्वतंत्र विचार व्यक्त करता है।
- “सीता गाना गाती है।”
- विश्लेषण: एक कर्ता (‘सीता’) और एक सकर्मक क्रिया (‘गाती है’) जिसका कर्म (‘गाना’) है। फिर भी, यह एक ही क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य है।
- “वर्षा हो रही है।”
- विश्लेषण: इसमें कर्ता छिपा हुआ है (यह), और केवल एक विधेय (‘वर्षा हो रही है’) है।
- “राम ने सेब खाया।”
- विश्लेषण: एक कर्ता (‘राम’), एक कर्म (‘सेब’) और एक क्रिया (‘खाया’)।
- “शिक्षक पढ़ा रहे हैं।”
- “सूरज चमक रहा है।”
- “मैंने पत्र लिखा।”
- “बाग में फूल खिले हैं।”
- “उसने दरवाज़ा खोला।”
सभी उपरोक्त वाक्यों में केवल एक क्रिया है और वे एक ही विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं।
२. संयुक्त वाक्य (Compound Sentence)
परिभाषा: जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य (स्वतंत्र उपवाक्य) योजक शब्दों (Conjunctions) के द्वारा आपस में जुड़कर एक बड़ा वाक्य बनाते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक शब्द जैसे- और, एवं, तथा, या, अथवा, पर, परन्तु, किन्तु, इसलिए, अतः, वरना, नहीं तो आदि।
विशेषताएँ:
- इसमें दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं।
- प्रत्येक उपवाक्य अपने आप में पूर्ण और सार्थक होता है।
- उपवाक्य योजकों द्वारा जुड़े होते हैं।
- यदि योजक हटा दिया जाए, तो अलग-अलग सरल वाक्य बन जाते हैं।
उदाहरण और विश्लेषण (क्यों है संयुक्त वाक्य?):
- “मैंने दरवाज़ा खटखटाया परन्तु कोई उत्तर नहीं मिला।”
- विश्लेषण: यह दो सरल वाक्यों से मिलकर बना है:
- सरल वाक्य 1: मैंने दरवाज़ा खटखटाया।
- सरल वाक्य 2: (मुझे) कोई उत्तर नहीं मिला।
- योजक ‘परन्तु’ ने इन्हें जोड़ा है। दोनों स्वतंत्र हैं।
- विश्लेषण: यह दो सरल वाक्यों से मिलकर बना है:
- “वह बाज़ार गया और उसने फल खरीदे।”
- विश्लेषण:
- वह बाज़ार गया।
- उसने फल खरीदे।
- योजक ‘और’ से जुड़े हैं।
- विश्लेषण:
- “तुम पढ़ाई करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे।”
- विश्लेषण:
- तुम पढ़ाई करो।
- तुम फेल हो जाओगे।
- योजक ‘अन्यथा’ से जुड़े हैं।
- विश्लेषण:
- “मैंने उसे बुलाया किन्तु वह नहीं आया।”
- “तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी?”
- “वह अमीर है फिर भी दुखी है।”
- “बारिश हो रही है इसलिए मैं घर पर रुकूँगा।”
- “सूरज निकला और आकाश साफ़ हो गया।”
- “पहले आप खाना खाओ, फिर टीवी देखना।” (यहाँ ‘फिर’ योजक का काम कर रहा है)
- “न तो राम आया और न ही श्याम आया।”
३. मिश्रित वाक्य (Complex Sentence)
परिभाषा: जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य (Main Clause) और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य (Subordinate Clause) हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य स्वतंत्र होता है जबकि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है और अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाता।
विशेषताएँ:
- इसमें कम से कम दो उपवाक्य होते हैं।
- एक उपवाक्य प्रधान/मुख्य होता है।
- एक या अधिक उपवाक्य आश्रित होते हैं।
- आश्रित उपवाक्य प्रायः जो, कि, क्योंकि, जब, जहाँ, यदि, तो आदि से शुरू होते हैं।
- आश्रित उपवाक्य को अगर अलग से लिख दें, तो उसका अर्थ अधूरा लगेगा।
उदाहरण और विश्लेषण (क्यों है मिश्रित वाक्य?):
- “जो लड़का दौड़ रहा है, वह मेरा भाई है।”
- विश्लेषण:
- प्रधान उपवाक्य: वह मेरा भाई है। (यह स्वतंत्र है और पूर्ण अर्थ देता है)
- आश्रित उपवाक्य: जो लड़का दौड़ रहा है। (यह ‘वह’ की विशेषता बता रहा है। इसे अलग लिखने पर इसका अर्थ अधूरा है।)
- यहाँ ‘जो’ आश्रित उपवाक्य का आरम्भ कर रहा है।
- विश्लेषण:
- “मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो।”
- विश्लेषण:
- प्रधान उपवाक्य: मैं जानता हूँ।
- आश्रित उपवाक्य: कि तुम झूठ बोल रहे हो। (यह ‘क्या’ जानता हूँ, यह बता रहा है। यह प्रधान उपवाक्य के बिना अधूरा है।)
- विश्लेषण:
- “जब आप आएंगे तब मैं चला जाऊंगा।”
- विश्लेषण:
- प्रधान उपवाक्य: (तब) मैं चला जाऊंगा।
- आश्रित उपवाक्य: जब आप आएंगे। (यह समय बता रहा है।)
- विश्लेषण:
- “यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे।”
- विश्लेषण:
- आश्रित उपवाक्य (शर्त): यदि परिश्रम करोगे।
- प्रधान उपवाक्य (परिणाम): (तो) सफल होगे।
- विश्लेषण:
- “वह स्थान जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर है।”
- “मैंने उसी डॉक्टर को दिखाया जिसने तुम्हारा इलाज किया था।”
- “क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए मैं बाहर नहीं गया।”
- “जैसे ही घंटी बजी, बच्चे कक्षा से बाहर आ गए।”
- “मैं उसे जानता हूँ जो यहाँ का मालिक है।”
- “यह वही कलम है जो मैंने कल खरीदी थी।”
संक्षेप में:
- सरल वाक्य: एक विचार, एक क्रिया।
- संयुक्त वाक्य: एक से अधिक स्वतंत्र विचार, योजकों द्वारा जुड़े।
- मिश्रित वाक्य: एक स्वतंत्र विचार + एक या अधिक आश्रित विचार।
वाक्य के तत्व:
प्रत्येक वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं:
१. उद्देश्य (Subject) – वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए
उद्देश्य के दो भाग होते हैं:
- कर्ता (क्रिया को करने वाला)
- कर्ता का विशेषण (कर्ता की विशेषता बताने वाला शब्द)
२. विधेय (Predicate) – उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए
विधेय के चार भाग होते हैं:
- क्रिया (कार्य या स्थिति का बोध)
- कर्म (जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े)
- पूरक (क्रिया का अर्थ पूरा करने वाला)
- विशेषण (क्रिया की विशेषता बताने वाला)
उदाहरण: “मेरा छोटा भाई सुबह से पुस्तकालय में किताबें पढ़ रहा है”
उद्देश्य: मेरा छोटा भाई
विधेय: सुबह से पुस्तकालय में किताबें पढ़ रहा है
वाक्य निर्माण के नियम:
१. कर्ता-क्रिया अन्विति – कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग
उदाहरण: “लड़कियाँ खेलती हैं” (न कि “खेलता है”)
२. शब्द क्रम – हिंदी में वाक्य की मूल संरचना: कर्ता + कर्म + क्रिया
उदाहरण: “राम रोटी खाता है” (न कि “रोटी खाता है राम”)
३. विराम चिह्नों का सही प्रयोग – अल्पविराम, अर्द्धविराम, पूर्णविराम आदि का उचित प्रयोग
४. वाच्य की एकरूपता – वाक्य में क्रिया का एक ही वाच्य में प्रयोग
५. अनावश्यक शब्दों का परिहार – वाक्य में ऐसे शब्द न हों जिनके बिना भी अर्थ स्पष्ट हो
विशेष तथ्य:
- वाक्य रचना में संस्कृत के ‘करता-कर्म-क्रिया’ क्रम का पालन करना चाहिए
- मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्य को प्रभावशाली बनाता है
- वाक्य की लम्बाई उचित होनी चाहिए, न अधिक लम्बा न अधिक छोटा
निष्कर्ष:
वाक्य विचार का ज्ञान भाषा की शुद्धता और प्रभावशीलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक अच्छा वाक्य वही है जो सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होते हुए भी पूर्ण अर्थ प्रकट करे। वाक्य रचना के नियमों का पालन करके हम अपने विचारों को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकते हैं।
अभ्यास के लिए:
१. ‘जब तुम आए तो मैं सो रहा था’ – वाक्य भेद बताइए
२. ‘वह धीरे-धीरे चलता है’ – उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए
३. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए: “तुम और सोहन _____ जाओ”
४. वाक्य शुद्ध कीजिए: “उसने कहा कि मैं कल आएगा”
वाक्य विचार का यह ज्ञान न केवल हमारी लेखन क्षमता को विकसित करता है बल्कि हमारे संवाद को भी अधिक प्रभावी बनाता है।
